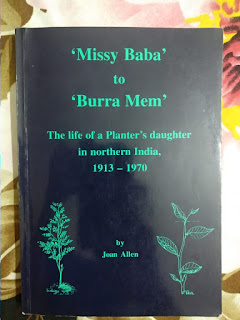सन 1878 ई
में प्रकाशित “लाइफ इन द मुफ्फसिल, ऑर,
द सिविलियन इन लॉअर बंगाल”(वॉल्यूम-1) किताब आईसीएस जॉर्ज ग्राहम
के भारत में उनके करियर के सफर के शुरुआती हिस्से और बंगाल खासकर तिरहुत जिले में
उनके अनुभवों का संस्मरण है। उनके करियरी सफर की शुरुआत होती है उन्नीसवीं शताब्दी
के सतरवें दशक से यानि सन 1857 की भारतीय क्रांति के कुछ सालों बाद से ही ... इसी कालखंड में इंग्लैंड में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में
नियुक्ति की शुरुआत हुई थी । जॉर्ज
ग्राहम इसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होकर भारत के अपने सफर की शुरुआत कर रहे
थे। शुरुआती सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए आए हुए ये सिविल सेवा के
अधिकारी भारत में पहले के अँग्रेज़ अधिकारियों के बीच तिरछी निगाहों से देखे जाते
थे। ... और इन अधिकारियों के लिए एक शब्द था- कंपीटिशनवाला। अभी सुनने में भले ही यह अजीब लगे , लेकिन तब
बाप-दादा-चाचा की सिफारिशों से आए `इलीट` इन्हें अपनी
तुलना में कमतर आंकते और इन्हें किताबी कीड़ा और घुसपैठिया समझते। और उनकी नजर में
चूंकि ये निदेशक द्वारा नामांकित नहीं थे या हेलीबेरी से पढ़कर नहीं निकले थे,
इसलिए इन कंपीटिशनवालों के तौर-तरीके उतने रिफांइड नही थे, जितने होने चाहिए औऱ यह
भी कि न तो ये ढ़ंग से घुड़सवारी कर सकते हैं और न ही ढ़ंग से निशानेबाजी।

जॉर्ज
ग्राहम समुद्री जहाज लेडी एलेनबोरो से एक सौ बयालीस दिन की यात्रा के बाद भारत
पहुंचे। तीन महीने के सफर का अनुमान था, लेकिन डाउंस
से कलकत्ता का उनका सफर करीब 5 महीने में पूरा हुआ । उनके आने तक सिविल सेवा में
आए अधिकारियों को अंदरुनी इलाकों में अपनी सेवा शुरु करने से पहले दो भाषाओं की
परीक्षा में सफल होना होता था। पंजाब, अवध और उत्तर-पश्चिम के प्रांतों के लिए
फारसी और हिंदी एवं बंगाल में सेवा के लिए
हिंदुस्तानी और बंगाली। परीक्षा मासिक तौर पर होती थी और एक समय में एक ही भाषा की
परीक्षा दी जा सकती थी । बोर्ड ऑफ एक्जामीनर्स
के द्वारा दूसरी भाषा की परीक्षा तब तक नहीं ली जाती थी ,जबतक कि पहले में आप पास
न हो गए हों। हालांकि इन नियमों में बाद में बदलाव किए गए।
जॉर्ज
ग्राहम साहब के हिस्से हिंदुस्तानी और बंगाली आयी। हिंदुस्तानी की सीख के लिए उनका
मुख्य टेक्स्ट बुक था- बाग-ओ-बहार और बंगाली के लिए बैताल पुंशविंशति उर्फ बैताल पच्चीसी- बैताल की पच्चीस कहानियां। सिविल
सेवा में आए ब्रिटिश अधिकारी इसके लिए पंजीकृत/चिह्नित मुंशियों के जरिए इन भाषाओं की समझ
विकसित करते। इन मुंशियों के लिए मुंशी अलावएंस का प्रावधान होता था। खैर जॉर्ज
ग्राहम साहब भाषाओं वाली परीक्षा में सफल हुए और अब बंगाल के अंदरुनी इलाकों में
काम करने के लिए एलीजिबल थे।
जॉर्ज साहब
ने लिखा है कि उन दिनों में जबकि बिछायी रेल-पटरियां आसानी से “गिनी” जा सकती थी, स्टेशन/कार्यालय ज्वाइन करने के समय के संबध में
पुराने नियम ही लागू थे।... यानि उनके लिए करीब एक सप्ताह तैयारी के लिए और पैंतीस
दिन यात्रा के लिए समय था । जॉर्ज ग्राहम को मुजफ्फरपुर पहुंचना था। तब तिरहुत
जिले का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में था और दरभंगा इसका सब-डिविजन जिसका मुख्यालय
दरभंगा शहर में न होकर उस समय बहेड़ा में था । भागलपुर तक करीब आधी दूरी रेल के
जरिए तय की। फिर भागलपुर से चार बैलगाड़ियों में सामान मुजफ्फरपुर के लिए रवाना
किया गया साथ ही उनके घोड़े भी कूच कर गए। फिर रेलवे वाली ट्रॉली के जरिए
सुल्तानपुर तक पहुंचे... फिर इंजन के जरिए जमालपुर तक... रेल की पटरियां अभी बिछ
ही रही थी। आगे पटना तक का सफर घोड़े और पालकी से तय किया उन्होंने।
जॉर्ज
ग्राहम ने लिखा है कि बिहार प्रांत छह जिलों में बंटा है , जिसका कुल क्षेत्रफल
23,732 वर्ग मील और 1872 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या 13,123,529 है, जिसका
प्रशासन पटना कमिश्नर के द्वारा देखा जाता है। पटना बिहार प्रांत का मुख्यालय है
और पटना कमिश्नर के ऊपर लेफ्टिनेंट-गवर्नर और उसके ऊपर भारत के गवर्नर-जनरल। और
हां रैंक और वेतन-भत्तों के लिहाज से उनके बाद ओपियम अजेंट का नंबर आता है ।
ग्राहम साहब ने पीडब्ल्यूडी का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस विभाग से बाहर के लोग
मजाक से इसे पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। ग्राहम साहब का पटना में
ठिकाना वहां का यूरोपीय इलाका बांकीपुर था।
भारतीय दंड
संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता लागू होने के अभी शुरुआती दिन थे। ऐसे में
पटना की एक पार्टी में सुनकर वो चौंक गए कि जब एक युवा अंग्रेंज पुराने सुनहरे
दिनों की मन मसोस कर याद कर था कि पहले कोई नौकर कैंटनमैंट के दायरे में कोई गलत
व्यवहार करता था तो उसे उसके मालिक-मालकिन एक नोट के साथ कैंटनमैंट मैजिस्ट्रेट के
पास भेज देता था कि पत्रवाहक को निर्धारित संख्या में बेंत लगाए जाए और उसका
अनुरोध मैजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार लिया जाता था लेकिन अब के दिनों में किसी
यूरोपीय की तरह स्थानीय लोगों के मामले में भी केस दर्ज कराना पड़ता है।
खैर ग्राहम
साहब पहले नाव के जरिए हाजीपुर और फिर घोड़े के जरिए मुजफ्फरपुर तक पहुंचे। जॉर्ज
ग्राहम ने मुजफ्फरपुर के बारे में विस्तार से बताते हुए लिखा है कि उत्तर की ओर
देखने पर बर्फ से लदी हिमालय की चोटियां भी धुंधली-धुंधली दिखाई देता है। दरभंगा राज का जिक्र
करते हुए उन्होंने लिखा है कि उस समय दरभंगा के राजा के कम उम्र की वजह से
जमींदारी सरकार की देखरेख में थी और अंग्रेज सरकार के द्वारा नियुक्त मैनेजर अपना
अधिकांश समय मुजफ्फरपुर के सिंकदरपुर में महलनुमा इमारत में ही अधिकांश समय बिताते
थे।
नई पुलिस
व्यवस्था अभी लागू नहीं हुई थी। जिला पुलिस कार्यक्षेत्र के नजरिए से थानों में
बंटा हुआ था, जिसका मुखिया दारोगा होता था, जिसके नीचे नायब यानि डिप्टी दारोगा और
फिर बरकंदाज यानि कॉस्टेंबल थे। थानों से दैनिक रुप से रिपोर्ट आती थी और ज्वाइंट
मैजिस्ट्रेट इसे देखते-सुनते थे।
नई दंड
संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता उस साल लागू हुई थी और मैजिस्ट्रेट के लिए
अपने हाथ से एवीडेंस अगंरेजी में नोट करना, स्थानीय भाषा में गवाह को उसे पढ़कर
सुनाना और फिर यह पूछना जरुरी था कि कि ये सही है या नहीं। शिकायतकर्ता के द्वारा
शपथ लिया जाने की प्रक्रिया को पूरा करना भी टेढ़ी खीर लगती थी। उन्होंने लिखा है
कि पहले जहां हिंदू गंगाजल , गाय की पूंछ और बड़े बेटे के सिर पर हाथ रखकर सच
बोलने की कसम लेते थे, वहीं अब उन्हें एक निश्चित शपथ लेनी पड़ती थी । हिंदू और
मुसलमान के नए शपथ में अंतर बस इतना था कि मुस्लिम धर्म की जगह इमाम बोलते थे वहीं
परमेश्वर की जगह खुदा। उन्हें तिरहुत के कलेक्टर साहब ने शुरुआती दिनों में ही
गुरु मंत्र दिया कि सिविल सेवा के अधिकारी सब कुछ पता होना चाहिए या फिर जताना
चाहिए कि उसे सब कुछ पता है।
जॉर्ज
ग्राहम ने लिखा है कि अदालत में गवाहों से जिरह करते हुए कुछ सवाल तय होते हैं और
गवाह भी उसी मुताबिक तैयार होकर आते थे। जैसे अमूमन पहला सवाल
होता है- क्या आप वादी के रिश्तेदार है , दूसरा- कौन पहले आया ... आप या दूसरे
गवाह। तीसरा कि जब घटना घटी तो आप किधर थे- उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम ।
उन्होंने लिखा है कि बायें और दाएं बोलने के बजाय यहां लोग पूरब या पश्चिम बोलते
है। एक बार वो जब शिकार पर निकले तो उनका चपरासी सिगार जलाने के लिए जला हुआ
गोइंठा या उपला लेकर आया । उनके सिगार का छोर ठीक से जला नहीं । चपरासी ने बोला
हाकिम सिगार को थोड़ा पश्चिम में कीजिए न।
उन्होंने
लिखा है हमलोगों पर अक्सर आरोप लगता है कि स्थानीय लोगों से मेलमिलाप की हमारी कोई
इच्छा नहीं होती , लेकिन ऐसे में कोई क्या मेल-मिलाप करेगा जबकि जबकि सामने वाले
को यह लगे कि वो हमारे छुने से ही अपवित्र हो गया है और वो उस खाद्य पदार्थ को
नहीं खाएगा, जिसपर हमारी छाया पड़ी हो। उन्होंने लिखा है कि दरभंगा महाराज जिनका
देहांत कुछ समय पहले हुआ है जो कि ठीक-ठाक अगंरेज अधिकारियों के संपर्क में रहते
हैं, उनके बारे में यह पता चला है कि वो
अग्रेंज अधिकारियों से मिलने के बाद वापस घर लौटने पर तुरंत कपड़े बदलते थे और
उन्हें तब तक दुबारा नहीं पहनते थे जब तक कि उसे अच्छी तरह से पवित्र न कर लिया
गया हो और साथ ही वे खुद को भी शुद्ध करते थे। उन्होंने अपने साथ हुई एक घटना का
भी जिक्र किया है। दरंभंगा के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के तौर पर वो एक सुबह किसी
गांव से गुजर रहे थे और मुखियाओं से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने जब पानी लाने के
लिए कहा और एक नए मिट्टी के बर्तन में उनके लिए पानी लाया गया। वो घोड़े पर बैठे
थे ।जब उन्होंने पानी पी लिया तो उनसे कहा गया कि बर्तन को दूसरी तरफ बचे हुए पानी
समेत फेंक दें । जिससे कि गांव में वो बर्तन दुबारा इस्तेमाल में न आ सके और न ही
पानी की कोई बूंद उन लोगों के करीब पहुंचे। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने थोड़ा सा
भी नहीं सोचा कि इससे मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैने उनके कहे अनुसार ही किया।
उन्होंने
लिखा है कि मुजफ्फरपुर में अधिकारियों के बीच की एक पार्टी में एक अँग्रेज़ डॉक्टर
ने उन्हें बताया कि उन्होंने उस दिन ऊंची जाति की एक महिला के पैर का ऑपरेशन उसे
देखे बिना किया ,सिवा उस हिस्से को छोड़कर जिसका उन्होंने ऑपरेशन किया। पर्दे में
एक छेद से महिला के पैर को डॉक्टर साहब की तरफ किया गया और एक ब्राहम्ण ने जो कि
दवाईओं के बारे में थोड़ा-बहुत जानता था क्लोरोफॉर्म के उपयोग में मदद की।
मुजफ्फरपुर
में उनके दिन ठीक-ठाक गुजर ही रहे थे कि ग्राहम साहब को दरभंगा सब-डिविजन का चार्ज
मिला। तब दरभंगा सब-डिविजन का मुख्यालय बहेड़ा से दरभंगा शहर में स्थानांतरण करने
की प्रक्रिया चल रही थी। दरअसल जब दरभंगा राज की जमींदारी कोर्ट ऑफ वार्ड के
प्रबंधन में आई तो यूरोपीय मैनेजर को दरभंगा में भी रहना पड़ता था और मैजिस्ट्रेट
कोर्ट के लिए बहेड़ा तक जाना उसे काफी असुविधाजनक लगता। उसने इस बात की सिफारिश की
कि चूंकि दरभंगा तिरहुत जिले का सबसे बड़ा शहर है ऐसे में कोर्ट का दरभंगा में ही
होना सही रहेगा। उसने मैजिस्ट्रेट के रहने और कोर्ट के लिए दो इमारत देने का भी
प्रस्ताव रखा। सरकार ने उसके सिफारिश और प्रस्तावों को मंजूरी दे दी और ग्राहम
साहब को दरभंगा जाने के लिए मिले आदेश के समय बहेड़ा से सब-डिविजन ऑफिस का सारा
तामझाम दरभंगा ले जाया जा रहा था।
जॉर्ज
ग्राहम साहब ने अपने संस्मरण में मुजफ्फरपुर में होने वाले सालाना मीट, नेपाल की
तराई के इलाके और मुजफ्फरपुर के पास शिकार के अनुभव और सोनपुर मेले के दौरान
यूरोपीय लोगों के मिलन समारोह का भी जिक्र किया है। लाइफ इन द
मुफ्फसिल, ऑर, द सिविलियन इन लॉअर बंगाल तत्कालीन बिहार को ब्रिटिश शासकीय दृष्टि से
समझने का , प्रशासन और समाज के संबंधों को जानने के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है।
जॉर्ज ग्राहम के अपने बायसेस हैं, स्थानीय लोगों की चर्चा करते है तो कई बार
श्रेष्ठता का उनका दंभ भी दिखता है और साथ-साथ ही उनकी स्वीकारोक्तियां भी है।